परिचय
प्राचीन भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्धिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल का दौर था, जिसे अक्सर "दूसरा शहरीकरण" या "अक्षीय युग" कहा जाता है। इस युग में कई नए धार्मिक और दार्शनिक आंदोलनों का उदय हुआ, जिन्होंने स्थापित वैदिक परंपराओं को चुनौती दी। इनमें से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुखता से उभरे, जिन्होंने आध्यात्मिक मुक्ति के लिए वैकल्पिक मार्ग पेश किए और भारत और उसके बाहर के धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। क्रमशः महावीर और सिद्धार्थ गौतम (बुद्ध) द्वारा स्थापित, इन श्रमण परंपराओं ने वेदों के अधिकार पर सवाल उठाए, उस समय के विस्तृत अनुष्ठानों और सामाजिक पदानुक्रमों की आलोचना की और व्यक्तिगत प्रयास, नैतिक आचरण और आत्मज्ञान की खोज पर जोर दिया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने आने वाली शताब्दियों के लिए इसके दार्शनिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रक्षेपवक्र को आकार दिया और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया।

पृष्ठभूमि
छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के सामाजिक-धार्मिक संदर्भ में वैदिक परंपराओं के विकास और समाज के कुछ वर्गों में बढ़ते असंतोष के बीच जटिल अंतर्संबंध की विशेषता थी। उत्तर वैदिक काल (लगभग 1200-500 ईसा पूर्व) में वर्ण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण देखा गया था, जिसमें ब्राह्मणों के पास महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक शक्ति थी। विस्तृत और महंगे अनुष्ठान, जिनमें अक्सर पशु बलि शामिल होती थी, वैदिक प्रथाओं का केंद्र बन गए थे। कर्मकांड और पदानुक्रमित सामाजिक संरचना पर इस जोर ने उन लोगों के बीच अलगाव और सवाल की भावना को जन्म दिया, जो आध्यात्मिक समझ और मुक्ति के लिए अधिक प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत मार्ग की तलाश कर रहे थे। रूढ़िवादी वैदिक परंपरा के साथ-साथ, श्रमण के रूप में जानी जाने वाली विभिन्न तपस्वी और घुमक्कड़ भिक्षु परंपराएँ मौजूद थीं। इन समूहों ने अक्सर वेदों के अधिकार को अस्वीकार कर दिया और ध्यान, योग और आत्म-त्याग जैसी प्रथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक जांच के अपने स्वयं के मार्गों का अनुसरण किया। बौद्धिक माहौल नए विचारों और वैकल्पिक विश्वदृष्टिकोणों के लिए परिपक्व था।
जैन धर्म का उदय
जैन धर्म की उत्पत्ति चौबीस तीर्थंकरों (आध्यात्मिक शिक्षक या "पार्क-निर्माता") की वंशावली से हुई है। चौबीसवें और सबसे हाल के तीर्थंकर, वर्धमान, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे, ऐतिहासिक रूप से महावीर ("महान नायक") के रूप में पहचाने जाते हैं। वर्तमान बिहार में एक शाही परिवार में जन्मे, महावीर ने आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में तीस वर्ष की आयु में अपने सांसारिक जीवन को त्याग दिया। उन्होंने बारह वर्षों तक कठोर तप किया, गंभीर कष्टों को सहन किया और गहन ध्यान किया। बयालीस वर्ष की आयु में, उन्होंने केवला ज्ञान (सर्वज्ञता) प्राप्त किया, एक जिन ("आंतरिक शत्रुओं का विजेता") और वर्तमान ब्रह्मांडीय युग के अंतिम तीर्थंकर बन गए।
जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएँ अहिंसा (अहिंसा), सत्य (सच्चाई), अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य (ब्रह्मचर्य) और अपरिग्रह (अपरिग्रह) के सिद्धांतों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। जैन धर्म सभी जीवन रूपों की पवित्रता पर जोर देता है, किसी भी जीवित प्राणी, यहाँ तक कि सबसे छोटे कीड़े को भी नुकसान पहुँचाने से बचने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की वकालत करता है। यह सिखाता है कि सभी आत्माएँ स्वाभाविक रूप से शुद्ध हैं और उनमें अनंत क्षमताएँ हैं, लेकिन यह क्षमता कर्म के संचय से अस्पष्ट हो जाती है, जिसे एक सूक्ष्म भौतिक पदार्थ के रूप में देखा जाता है जो कार्यों और विचारों के माध्यम से आत्मा से जुड़ा रहता है। जैन धर्म का लक्ष्य कठोर आत्म-अनुशासन, तप और पाँच व्रतों के पालन के माध्यम से संचित कर्मों को त्याग कर आत्मा को शुद्ध करना है, अंततः मोक्ष (जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति) प्राप्त करना है। जैन धर्म बाद में दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया: दिगंबर (आकाश-वस्त्रधारी), जो पूर्ण नग्नता का अभ्यास करते हैं, और श्वेतांबर (सफेद वस्त्रधारी), जो सफेद वस्त्र पहनते हैं।
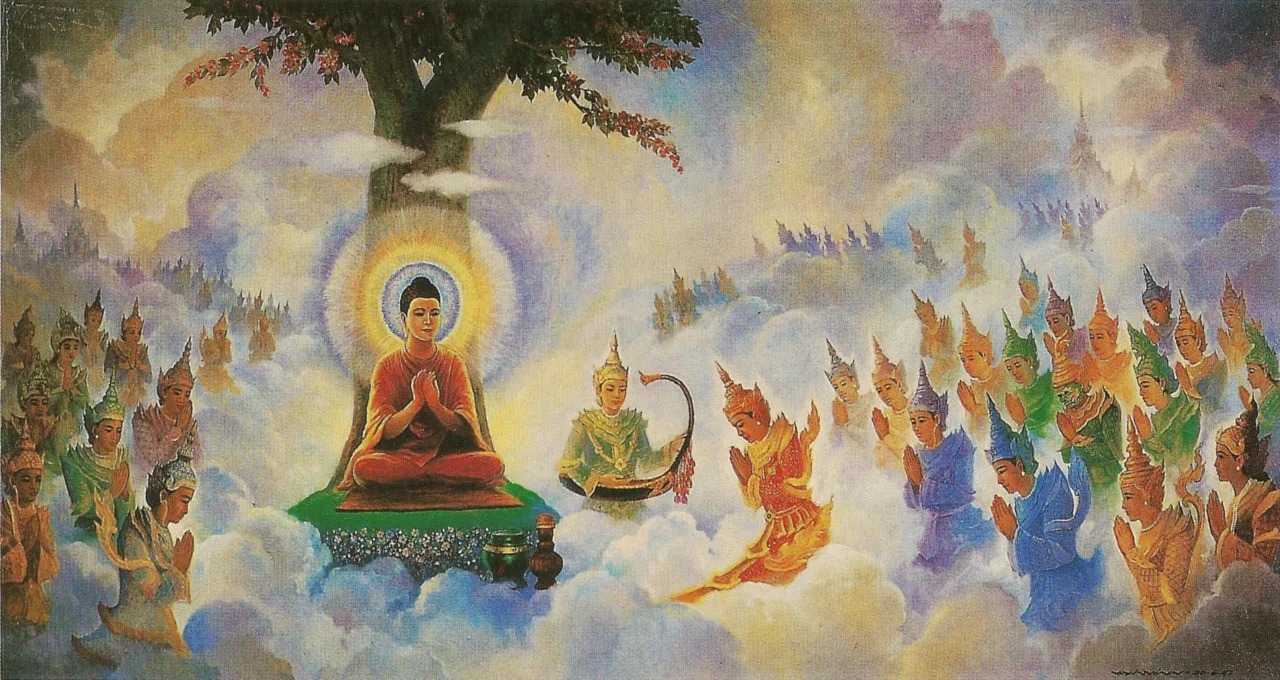
बौद्ध धर्म का उदय
बौद्ध धर्म की उत्पत्ति सिद्धार्थ गौतम से हुई, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे। कपिलवस्तु (वर्तमान नेपाल) में एक शाही परिवार में जन्मे सिद्धार्थ को उनके शुरुआती जीवन में दुनिया के दुखों से दूर रखा गया था। हालाँकि, बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु और एक तपस्वी का सामना करने पर, वह मानव अस्तित्व में निहित नश्वरता और पीड़ा से बहुत परेशान हो गए। उनतीस वर्ष की आयु में, उन्होंने अपने विशेषाधिकार प्राप्त जीवन को त्याग दिया और आत्मज्ञान की खोज में लग गए। उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न प्रकार के तप का अभ्यास किया, लेकिन अंततः उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक आत्म-त्याग से मुक्ति नहीं मिलती। फिर उन्होंने "मध्य मार्ग" अपनाया, जो अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या के बीच संयम का मार्ग था।
पैंतीस वर्ष की आयु में, बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध ("जागृत व्यक्ति") बन गए। उनकी मुख्य शिक्षाएँ चार आर्य सत्यों में समाहित हैं: (1) दुख (दुख मौजूद है), (2) समुदाय (इच्छाओं से आसक्ति के कारण दुख उत्पन्न होता है), (3) निरोध (इच्छाओं से आसक्ति समाप्त होने पर दुख समाप्त हो जाता है), और (4) मग्गा (आठ गुना मार्ग का अनुसरण करके दुख समाप्त किया जा सकता है)। आठ गुना मार्ग में सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही एकाग्रता शामिल हैं। जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म भी कर्म की अवधारणा और पुनर्जन्म के चक्र पर जोर देता है। बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, जो दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की स्थिति है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म बाद में विभिन्न स्कूलों में विकसित हुआ, जिनमें सबसे उल्लेखनीय थेरवाद (बुजुर्गों का स्कूल) और महायान (महान वाहन) थे।
वैदिक परम्पराओं के लिए चुनौतियाँ
जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय ने उस समय की स्थापित वैदिक परंपराओं के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। दोनों धर्मों ने वेदों के अधिकार को ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित ग्रंथों के रूप में अस्वीकार कर दिया। उन्होंने वैदिक प्रथाओं के केंद्र में मौजूद विस्तृत और अक्सर महंगे अनुष्ठानों और पशु बलि की आलोचना की, आध्यात्मिकता के लिए अधिक व्यक्तिगत और नैतिक दृष्टिकोण की वकालत की। इसके अलावा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने वर्ण व्यवस्था की कठोरता और अंतर्निहित असमानताओं का विरोध किया। उन्होंने उपदेश दिया कि आध्यात्मिक मुक्ति सभी सामाजिक स्तरों के व्यक्तियों के लिए सुलभ है, चाहे उनका जन्म कुछ भी हो। नैतिक आचरण, अहिंसा और व्यक्तिगत प्रयास पर उनका जोर कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जो मौजूदा सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था से हाशिए पर या मोहभंग महसूस करते थे।
सामाजिक प्रभाव और संरक्षण
जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्राचीन भारत में गहरा सामाजिक प्रभाव था। उनकी शिक्षाएँ, जो करुणा, अहिंसा और समानता पर जोर देती थीं, ने लोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित किया, जिसमें निम्न सामाजिक वर्ग और महिलाएँ शामिल थीं, जिन्हें अक्सर प्रमुख वैदिक प्रथाओं से बाहर रखा जाता था। दोनों धर्मों के लिए मठवासी आदेशों (संघों) की स्थापना ने व्यक्तियों को सांसारिक जीवन को त्यागने और अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए खुद को समर्पित करने के अवसर प्रदान किए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को विभिन्न शासकों और धनी व्यापारी समुदायों से भी महत्वपूर्ण संरक्षण प्राप्त हुआ। मगध साम्राज्य के बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजाओं को बुद्ध और महावीर दोनों का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के समर्पित प्रयासों के साथ-साथ इस शाही संरक्षण ने भारतीय उपमहाद्वीप में इन नई धार्मिक परंपराओं के प्रसार और स्थापना में मदद की।

समानताएं और भेद
जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कई समानताएँ थीं, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्धिक और आध्यात्मिक माहौल को दर्शाती हैं। दोनों की उत्पत्ति श्रमण परंपरा में हुई, कर्म और पुनर्जन्म के महत्व पर जोर दिया, दुख के चक्र से मुक्ति का लक्ष्य रखा और नैतिक आचरण और तपस्वी प्रथाओं के जीवन की वकालत की। हालाँकि, वे अपनी मूल शिक्षाओं और प्रथाओं में भी भिन्न थे। जैन धर्म ने चरम तप और अहिंसा पर जोर दिया, जिसमें सल्लेखना (मृत्यु तक उपवास) जैसी प्रथाएँ शामिल थीं। बौद्ध धर्म ने भोग और आत्म-पीड़ा दोनों की अति से बचते हुए मध्यम मार्ग की वकालत की। जहाँ जैन धर्म एक शाश्वत आत्मा (जीव) के अस्तित्व को मानता है, वहीं बौद्ध धर्म एक स्थायी, अपरिवर्तनीय आत्म (अनत्ता) की अवधारणा को नहीं मानता। निर्वाण और मोक्ष के बारे में उनकी समझ भी सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से भिन्न थी।
प्रभाव और महत्व
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय भारतीय और विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। इन आंदोलनों ने न केवल वैकल्पिक धार्मिक और दार्शनिक प्रणालियाँ पेश कीं, बल्कि उस समय के सामाजिक और नैतिक परिदृश्य को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। अहिंसा, करुणा और नैतिक जीवन पर उनके जोर ने भारतीय संस्कृति पर एक स्थायी प्रभाव डाला है और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करना जारी रखा है। उन्हें मिले संरक्षण ने इन परंपराओं से जुड़ी कला, वास्तुकला और साहित्य को समृद्ध किया। प्रमुख वैदिक व्यवस्था के लिए उन्होंने जो चुनौती पेश की, उससे हिंदू धर्म के भीतर ही बौद्धिक बहस और सुधार का दौर शुरू हो गया।

परंपरा
जैन धर्म और बौद्ध धर्म की विरासत आधुनिक दुनिया में महत्वपूर्ण बनी हुई है। जैन धर्म, हालांकि एक छोटे से अनुयायी के साथ, भारतीय नैतिकता को गहराई से प्रभावित करता है और अहिंसा और तप के अपने सख्त सिद्धांतों को कायम रखता है। बौद्ध धर्म, भारत में सदियों तक फलने-फूलने के बाद, पूरे एशिया में फैल गया और एक प्रमुख विश्व धर्म बन गया, जिसने वैश्विक स्तर पर दर्शन, मनोविज्ञान और माइंडफुलनेस प्रथाओं को प्रभावित किया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन दो परंपराओं का उदय अर्थ, मुक्ति और जीवन के अधिक नैतिक तरीके के लिए स्थायी मानव खोज का प्रमाण है।

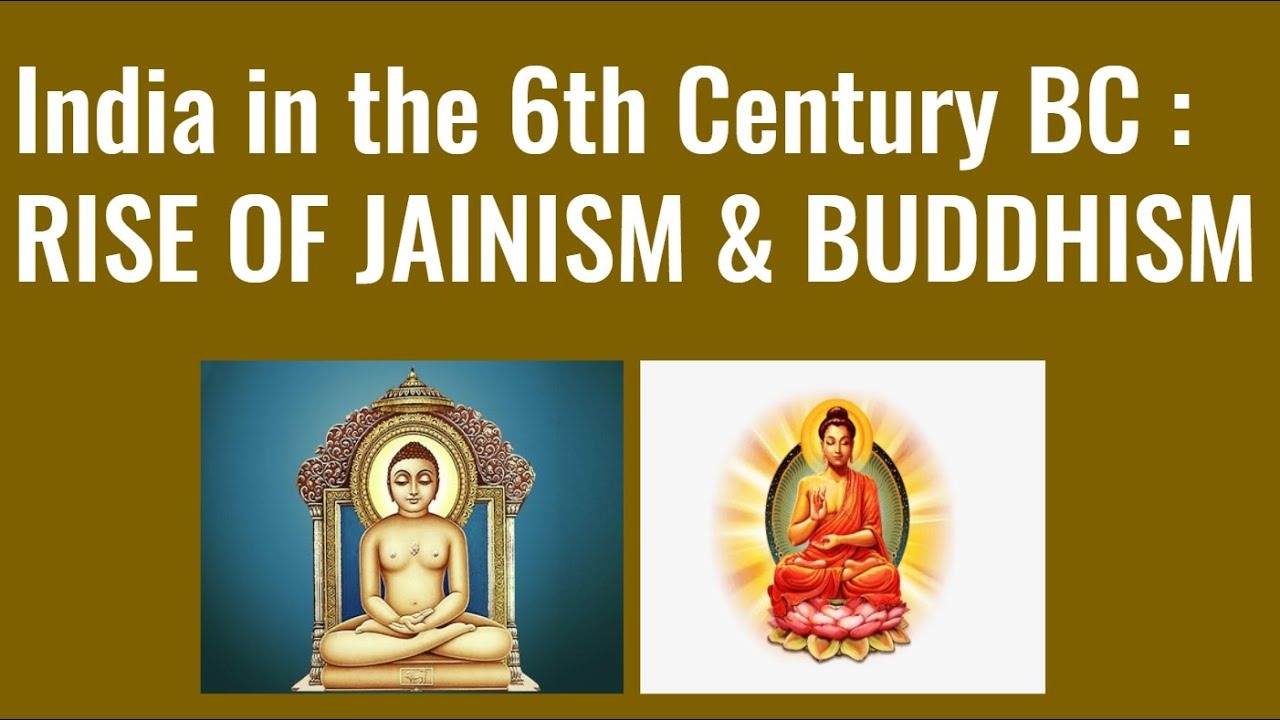
इस बारे में प्रतिक्रिया दें